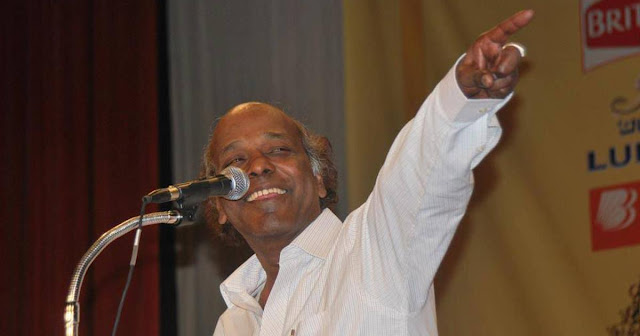पिछले दिनों नामवर सिंह पर हिन्दी के `विद्वानों` के ताबड़तोड़ लाइव कार्यक्रमों के दौरान किसी ने उनके संपादन में `आलोचना` का पुनर्प्रकाशन शुरू होने पर पहला अंक (फ़ासीवाद और संस्कृति का संकट') फ़ासीवाद पर केंद्रित किए जाने को उनकी प्रमाणिकता के तौर पर पेश किया था। इस अंक पर 2000 में छपी आलोचक कृष्ण मोहन की विस्तृत समीक्षा (उदारवादी भ्रमों का पुलिंदा - आलोचना का फ़ासीवादी अंक) पढ़ी। यह अंक `फ़ासीवाद संबंधी लेखों का दिशाहीन और भ्रामक ढेर` क्यों है, इस पर उन्होंने गंभीरता से विभिन्न लेखों के उदाहरण सामने रखते हुए विचार किया है। यूँ यह एक ज़रूरी बात है कि लेखक जैसा समझता है, उसे ईमानदारी से लिखे पर जैसा कि साहित्य की दुनिया का पावर स्ट्रक्चर है और जवाब में विमर्श के बजाय हिसाब चुकता करने का रिवाज़ है, एक साथ इतने सारे प्रभावशाली और फ़ितरती लेखकों से बेबाकी के साथ तीखी असहमति व्यक्त करन साहस की बात है।
बेहतर तो यह होता कि इस लेख से एक के बाद एक कई हिस्से यहाँ उद्धृत करता या पूरा लेख ही यहाँ देता। फ़िलहाल, लंबा टाइप न कर पाने की स्थिति से यह संभव नहीं है। आलोचना के फ़ासीवादी अंक में एजाज़ अहमद के एक पूर्व प्रकाशित लेख को भी शामिल किया गया था जिसे कृष्ण मोहन सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय मानते हैं और पर विस्तार से बात करते हुए अपनी असहमतियां भी जताते हैं। लेकिन खिन्नता पैदा करने वाले वे हिस्से हैं जिन्हें हिन्दी के विद्वानों के लेखों से लिया गया है। यह अंक `आलोचना` का है लेकिन जो विशेषांक लेखक संगठनों द्वारा निकाले जाते रहे हैं, उनमें भी यही लेखक अपनी फ़ासिस्ट समर्थक, कम्युनल, सेमी-कम्यूनल या सवर्ण अवधारणाओं के साथ उपस्थित रहते आए हैं और सर्व-स्वीकार्य रहे हैं। कृष्ण मोहन इस अंक के संपादक और प्रभाष जोशी के `रेनेसां पर्सन` नामवर सिंह की `मासूम` शिकायत का ज़िक्र भी करते हैं कि पटेल तो नेहरु की बात मान लेते थे पर अटल की बात आड़वाणी नहीं मानते। जसम के विचारक रविभूषण आरएसएस द्वारा ही पेश किए जाते रहे जुमले `वस्तुत; संघ परिवार जिस `हिन्दुत्व``को धर्म मानता है, वह एक जीवन-शैली है`, दोहरा रहे हैं। उनके लेख से ऐसे वाक्य उद्धृत कर कृष्ण मोहन जो सवाल उठाते हैं, वे असल में हिन्दी के पूरे बौद्धिक समाज से हैं। प्रभाष जोशी फ़ासीवाद से लड़ने के लिए सनातन धर्म का सहारा लेने और संघ के स्वयंसेवकों से प्रेरणा लेने की सीख देते हैं।
खगेंद्र ठाकुर के लेखन का अद्भुत कमाल तो
जलेस के `1857 पर आए विशेषांक` में देखा था। भारतेंदु की जिन पंक्तियों को फेरबदल कर रामविलास शर्मा ने 1857 से जोड़ दिया था, उनका असल रूप वीरभारत तलवार सप्रमाण हिन्दी वालों के सामने रख चुके थे पर
खगेंद्र ठाकुर ने उन्हें बदले हुए रूप में ही इस्तेमाल किया। अकारण नहीं कि ऐसे
झूठे उद्धरणों और विवादित अवधारणाओं से भरा वह (खगेंद्र ठाकुर का) लेख, उस अंक के कुछ बेहतरीन लेखों का प्रतिपक्ष ही था। फ़ासीवाद सम्बंधी `आलोचना` में छपे खगेंद्र ठाकुर के लेख से कृष्ण मोहन ने कुछ उद्धरण देते हुए लिखा है,-
``खगेंद्र ठाकुर और उनके भाकपाई मित्रों की यह पुरानी कमज़ोरी है कि वे शासक वर्ग से बार-बार उसका अंध-राष्ट्रवादी हथियार उधार मांगते हैं ताकि वे उनसे भी बड़े `राष्ट्रवादी` दिखें और एक ही झटके में पूरे राष्ट्र के नेता बन जाएँ।``
राजकिशोर के लेख से उद्धृत अंश देखिए- ``दुर्भाग्य यह
है कि इतिहास फ़ासीवादियों के साथ है। भारत में मुस्लिम शासन के बारे में
सेकुलरवादियों का नज़रिया साफ़ नहीं है। वे यह नहीं देख पाते कि शासन जैसा भी रहा
हो, मूलत:
एक अल्पसंख्यक शासन था। भारत की बहुसंख्या हिन्दुओं की थी,
अत: यहाँ का
सामंतवाद भी हिन्दू सामंतवाद होना चाहिए।``
इस पर कृष्ण
मोहन टिप्पणी करते हैं-
``मध्यकाल के बारे में औपनिवेशिक इतिहास लेखन की इसी साम्प्रदायिक दृष्टि में साझा करने के कारण उदारवाद अपने को कट्टरवाद के सामने कुंठित पाता है। उसे लगता है कि एक बार इस दृष्टि को सर्वस्वीकृति मिल जाए तो वह अपने ही जैसे उदार हिन्दू मन को भूल जाने और माफ़ करने के लिए मना लेगा। उसका सरल चित्त यह नहीं समझ पाता कि वह जितनी बार इस झूठ को शिरोधार्य करता है, उतनी ही बार कट्टरवादी शक्तियों को बल प्रदान करता है। उसकी वह मांग संघ परिवार की उस बुनियादी मांग से अलग नहीं है कि अगर अयोध्या, काशी, मथुरा पर उनका दावा मान लिया जाए तो वे बाकी मसले छोड़ देंगे। सामंतवाद सिर्फ़ सामंतवाद होता है। वह हिन्दू या मुस्लिम नहीं होता। और वह अनिवार्यत: अल्पसंख्यक का शासन होता है। राजकिशोर आधुनिकता की बातें बहुत करते हैं लेकिन धर्म के परदे के पार कुछ देख नहीं पाते। उनकी उदारता उन्हें बहुसंख्यकवाद की वक़ालत तक ले जाती है जो फ़ासीवादियों का एक प्रिय तर्क है। वे इतिहास की न्यूनतम आवश्यक छानबीन भी नहीं करते वरना उनके विश्वास भी ख़ुद ब ख़ुद खंडित हो जाते। संख्या की दृष्टि से उन्हें लगता है कि शासन तंत्र में मुसलमानो का बहुमत होता होगा जबकि मध्यकाल के सबसे मजहबी माने जाने वाले शासक औरंगेजेब के समय उसके सामंतों में लगभग अस्सी प्रतिशत हिन्दू थे।``
कृष्ण मोहन के लेख से ही हमें विष्णु खरे के इस `जागरूक समर्थन` का पता चलता
है - ``सिनेमा, टी.वी. में भारतीय
मानव-मूल्य बनाए रखने का बीजेपी का नारा भी प्रबुद्धता से फ़ासिज़्म-विरोध के पक्ष
में लेने में कोई हर्ज नहीं है। उनका हिंसा और सेक्स में डूबी अमेरिकी फिल्मो के
विरोध का हमें जागरूक समर्थन करना चाहिए।``
खरे के इस आह्वान पर कृष्ण मोहन लिखते हैं, ``इसे कहते हैं प्रबुद्धता और जागरूकता। सिनेमा में `भारतीय` मूल्यों को बचाने के भाजपाई नारे का समर्थन! हिंसा और अश्लीलता अमरीकी मूल्य हैं, भारतीय
समाज में हिंसा और अश्लीलता कहाँ। भारतीय संस्कृति के स्वयंभू, लंपट ठेकेदारों के
सुर में सुर मिलाने वाले खर साहब किसे धोखा देने चले हैं। सवाल यह है कि भारतीय
फ़ासीवाद के सांस्कृतिक एजेंडे का समर्थन करने वाला यह लेख कहीं आलोचना की
संपादकीय नीति का हिस्सा तो नहीं है।``
जाहिर है कि इस अंक के संपादक नामवर सिंह की नीति तो कहीं ज़्य़ादा भयानक रही ही है। खरे के बाद के हुसेन पर लिखे गए हमलावर लेख को `अरे, उन्हें क्या हुआ` कहकर हैरान होने वालों को इस टिप्पणी में उनके दिल-दिमाग़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मीर पर उनके लिखे को भी। इस टिप्पणी में उनके तर्क के आधार पर तो यह भी लगता है कि वे आज होते तो बॉलीवुड में दीपिका वगैराह के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाइयों के `जागरूक समर्थन` में भी खड़े मिल सकते थे।
भगवान सिंह हिन्दी के वामपंथियों के प्रिय लेखक रहे हैं और अपने खुले
साम्प्रदायिक लेखन के बावजूद अभी भी हैं। नामवर के फ़ासीवाद सम्बंधी अंक में वे न
हों और अपने इसी रंग में न हों तो इस अंक की सार्थकता ही भला क्या होती? कृष्ण मोहन लिखते हैं-
``भगवान सिंह ने
अपने लेख में मार्क्सवाद को दुनिया का सबसे नया, वैज्ञानिक और प्राधिकारवादी धर्म
माना है तथा `एक ही सामाजिक
वातावरण में उपजे होने के कारण` इसे ईसाइयत औऱ
इस्लाम के समतुल्य कहा है। साम्प्रदायिकता की आलोचना करने के लिए उन्होंने
मार्क्सवादियों की खिंचाई की है। उनका ख़याल है कि इसी वजह से साम्प्रदायिक
पार्टियों की ताक़त बढ़ी है। बाबरी मस्जिद के ध्वंस को वे दुर्भाग्यपूर्ण मानते
हैं, लेकिन `राजनीतिक लाभ` के लिए उसकी बरसी मनाने को उससे अधिक
दुर्भाग्यपूर्ण। वे मुसलमानों को भारत में अल्पपसंख्यक नहीं मानते और चिंता व्यक्त
करते हैं कि अगर यही रवैया रहा तो भारत में ख़ुद हिन्दू ही अल्पसंख्यक हो जाएँगे।
यह लेख शुरू से अंत तक ऐसी ही भ्रामक अवधारणाओं और आत्ममुग्ध लफ़्फ़ाज़ी से भरा
पड़ा है।``
असल में भगवान सिंह के लेख की ये अवधारणाएं और `आत्ममुग्ध लफ़्फ़ाज़ी` उनकी अपनी हैं ही नहीं। `मार्क्सवाद भी ईसाइयत और इस्लामियत के समतुल्य धर्म है` या `भारत में ख़ुद हिन्दू ही अल्पसंख्यक हो जाएँगे` जैसी बातें आरएसएस के प्रचारकों के `बौद्धिकों` में प्रमुखता से बताई जाती रही हैं। यहाँ तक कि ऐसे वचनों की कवरेज मैंने ही कई बार की है। यह बात अलग है कि हिन्दी के वामपंथी कवि-लेखक यह जानना-मानना नहीं चाहते हैं।
एक ज़माने के वामपंथी और साम्प्रदायिकता विरोधी कार्यशालओं के आयोजक पुरुषोत्तम
अग्रवाल इन दिनों मुख्य रूप से कबीर विशेषज्ञ हैं। नामवर सिंह पर लाइव श्रृंखला में
ही कुछ महीने पहले रामजन्मभूमि शिलान्यस की वेला में उन्होंने घोषणा की थी कि `गुरुजी` की इच्छा के
अनुरूप उनकी अगली किताब तुलसी पर होगी। यूँ, कबीर भी उनके लिए तुलसी ही हैं। इस
बात को आलोचना के फ़ासीवाद अंक के कबीर खंड में छपे पुरुषोत्तम अग्रवाल के लेख पर
कृष्ण मोहन की यह टिप्पणी पढ़कर समझा जा सकता है-
पुरुषोत्तम अग्रवाल कबीर की कविता को दलितों की पहचान के साथ जोड़ने को अस्मितावाद क़रार देते हुए उसे मूलत: आध्यात्मिक अनुभव की कविता कहते हैं। ``कवि कबीर की संवेदना का सत्य है वह अमरलोक जिसकी कसौटी पर वे जगत के तथ्य को कसते हैं…इस असीमित ब्रह्मांड में अपनी असीमित सत्ता के साथ होने का अनुभव;इस सीमित सत्ता के निस्सीम ब्रह्मांड के साथ सम्बद्ध होने की महिमा का अनुभव। ` `शंभुनाथ ने अपने लेख में समग्र का अंश होने के जिस अनुभव को सामाजिक अनुभव माना है और कबीर की कविता की रहस्यवादी व्याख्या से इनकार किया है, उस श्री अग्रवाल अध्यात्म की चाशनी में लपेटते हैं। इसका नतीज़ा निकालते हुए वे कहते हैं, ``कबीर अपने ख़ास दो-टूक ढंग से बताते हैं कि अनुभव का अपरिहार्य, अंतिम सत्य है मृत्यु। एक नाम-अनाम ही नित्य है बाक़ी सब अनित्य।`` श्री अग्रवाल ने अपने लेख में जिन यथास्थितिवादी आचार्यों को बार-बार कबीर निंदा का दोषी ठहराया है उनका भी विरोध कबीर के सामाजिक सरोकारों से ही था। हाँ, वे इतने कुशल अवश्य ही नहीं थे कि कबीर के नख-दंत तोड़कर उन्हें अपने ब्राह्मणवादी प्रोजेक्ट में शामिल करने की सोचते।
`परख` में छपा यह लेख `आलोचना` में छपता तो क्या हिन्दी विद्वानों,
विद्यार्थियों और शोधार्थियों का नज़रिया अपने इन विद्वानों को लेकर कुछ अलग होता? नहीं, क्योंकि ऐसी बातें या तो कही नहीं जातीं और कही जाती
हैं तो उन पर चर्चा नहीं की जाती। यह भी कह दिया जाता है कि ऐसी बातें लड़ाई को
कमज़ोर करती हैं। हालांकि, रघुवीर सहाय की पंक्ति ``अगर
वही हो तुम जिससे तुम लड़ते हो तो लड़ते क्यों हो`` उनके सामने होती है। इस लेख
का महत्व यही है कि बातें कही ज़रूर गई थीं। नामवर सिंह और उनके संपादन में निकले
उस अंक की याद में `आलोचना` के वर्तमान संपादक चाहें तो इस लेख को अब प्रकाशित कर सकते
हैं।