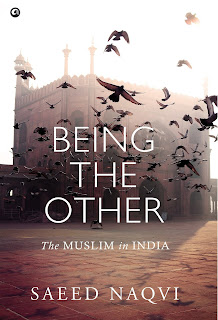(सईद नक़वी की पुस्तक ‘बीइंग दि अदर: दि मुस्लिम इन इण्डिया` (अलिफ़ बुक कंपनी, 2016) के एक अध्याय ‘ग्रोइंग अप इन अवध’’ का हिस्सा )
अनुवाद और प्रस्तुति : भारतभूषण तिवारी
हमारे समरसतापूर्ण अस्तित्व और मुक्त सांस्कृतिक अंतर्मिश्रण के चलते 1947 में हुए बँटवारे का दर्द कुछ गहरा था क्योंकि घनिष्ठता से जुड़े कुनबे भी अकस्मात् बंट गए. यह ज़िन्दगी की एक दर्दनाक विडम्बनाओं में से एक है कि हमारी इतनी अच्छी ख़ाला-नानी, नानी अम्मी, जिन्होंने हमेशा मुस्तफ़ाबाद में दफ़नाए जाने का ख़्वाब देखा था, लाहौर में अल्लाह को प्यारी हुईं. उनका शरीर हिंदुस्तान वापिस नहीं लाया जा सका और हम उनके जनाज़े में शरीक नहीं हो सके. आज के दौर में, जहाँ छोटे परिवार बढ़ते जाते हैं, ख़ाला-नानी शायद दूर की रिश्तेदार लगे, मगर हमारे परिवार में ऐसा नहीं था जो कि पारम्परिक संयुक्त परिवार व्यवस्था पर आधारित था. मेरी अम्मी की अम्मी अपने कुनबे में सबसे बड़ी थीं और नानी अम्मी सबसे छोटी. मेरी अम्मी से उनका ख़ास लगाव था जिनकी निगहबानी में वह बड़ी हुई थीं. इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि नानी अम्मी के अपने बच्चों का ख़याल न रखा गया हो; एक दूसरे पर अत्यधिक आश्रित रहने वाली उस व्यवस्था में उनके अपने बच्चों का ख़याल औरों ने रखा. दरअसल, जैसा कि मैंने पहले बताया, मुस्तफ़ाबाद का हमारा घर ममेरे-फ़ूफ़ेरे-मौसरे भाई-बहनों, मामियों-मौसियों-फूफियों और मामाओं-फ़ूफ़ाओं-मौसियों से भरा रहता (जिनकी तादाद मुहर्रम, बच्चा पैदा होने, किसी की मौत होने या शादी-ब्याह के मौकों पर सौ तक पहुँच जाती).
अपने इंतकाल के दिन तक नानी अम्मी को पासपोर्ट नामके दस्तावेज़ को समझने में बेहद मुश्किल हुई. वह इस इल्म के साथ बड़ी हुई थीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ़क़त रेलगाड़ी के टिकट की दरकार होती है. यह बात आसानी से समझ में आती है क्योंकि पहले की उनकी सारी यात्राएँ यूपी में अवध तक सीमित रहीं. वह बाराबंकी में पैदा हुईं, बिलग्राम में ब्याहीं और मुस्तफ़ाबाद या लखनऊ मेरे माता-पिता से मिलने आती रहीं. फिर बँटवारा हुआ, उसके बाद ज़मींदारी प्रथा का ख़ात्मा और फिर उनके शौहर का इंतकाल जो एक छोटे-मोटे सामंत थे. बाराबंकी और बिलग्राम के घर जीण-शीर्ण हालात में थे. नानी अम्मी हमारे साथ रहने आ गईं और मुस्तफ़ाबाद और लखनऊ के बीच आना-जाना करती रहीं.
पासपोर्ट की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी थी कि उनकी दो बेटियाँ पाकिस्तान में ब्याहीं और वहीं रह गईं. उनकी कश्मकश उतनी ही शदीद थी जितनी टोबा टेक सिंह की (सआदत हसन मंटो का एक काल्पनिक चरित्र) जो यह नहीं समझ पाया कि बँटवारा होने पर उसका गाँव पाकिस्तान में कैसे ‘जा’ सकता है; उसी तरह नानी अम्मी नहीं समझ पाईं कि उनकी बेटियाँ दूसरे मुल्क कैसे ‘जा’ सकती हैं. कोई अपना घरबार हमेशा के लिए कैसे छोड़ सकता है? उन्हें दिलासा देने की कोशिश में यह बतलाया गया कि उनकी बेटियाँ, सुग़रा और सकीना, वाकई घर छोड़ कर नहीं जा रही हैं. बम्बई में उनकी लड़कियों के वास्ते दो ‘बहुत अच्छे लड़के’ थे, मगर लाहौर लखनऊ से बेहद करीब था. तिस पर वे ‘लड़के’ (जिन्हें पाकिस्तान के कुछ कज़िन ने ढूँढा था) बहुत अच्छी ‘ज़ात’ के थे. ( उपमहाद्वीप के मुसलमानों पर हिन्दू जाति प्रथा के असर को कभी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. सैयद, शेख़, पठान अब भी ऊँची जातियाँ हैं और जुलाहे और दीगर पेशेगत श्रेणियों को नीचा माना जाता है.)
हिंदुस्तान का नक्शा निकाल कर बिछाया गया. नानी अम्मी को दिखाया गया कि कैसे त्रिवेंद्रम, मद्रास, बैंगलोर, हैदराबाद, बम्बई ये सब हिंदुस्तान में होते हुए भी लखनऊ से लाहौर क्या कराची से भी ज़्यादा दूर थे. उन्हें बतलाया गया की हिंदुस्तान-पाकिस्तान की सरहद महज एक बनावटी सरहद थी जिसे चंद हफ़्तों में एक ‘अंग्रेज़’ सर सिरिल रैडक्लिफ ने जल्दी-जल्दी में खींच दिया था, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की सरहद का फैसला करने के लिए मुकर्रर लिए गए दो कमीशनों के मुखिया थे. वक़्त के साथ-साथ सरहद ख़त्म हो जाएगी और वह उसे एक अस्थायी असुविधा के तौर पर ही लें.
इसलिए नानी अम्मी सुग़रा और सकीना को पाकिस्तान के ‘लड़कों’ से ब्याहने को राज़ी हो गईं. मगर जल्दी ही वह उनके शुरूआती शुबहों से रूबरू हुईं जो शुरुआत थी मोहभंग की. उनकी हसरत थी कि वह अपनी बेटियों के पास लाहौर जाएं और उन्हें पासपोर्ट हासिल करने को कहा गया. अगर लाहौर और कराची हिंदुस्तान के दीगर बड़े शहरों के मुकाबले लखनऊ से नज़दीक थे तो फिर क्यों उन्हें रेलगाड़ी के टिकट के अलावा एक और ‘टिकट’ लेने के लिए क्यों कहा जा रहा है. इस ‘अजीब’ ज़रूरत के पीछे की वजहों को उन्हें समझाने की कोशिशें की गईं, फिर पासपोर्ट के फॉर्म लाए गए और उन्होंने अचरज के साथ अपनी साफ़ उर्दू लिखावट में उन्हें भरा. मोहभंग का दूसरा मौक़ा आया. मेरे पिता के मुंशी ने उन्हें बतलाया कि अगर फॉर्म हिंदी या अंग्रेज़ी में भरा जाए तो उन्हें पासपोर्ट जल्दी मिल जाएगा. क्या उर्दू का कोई मोल नहीं रहा? उन्होंने पूछा.
नानी अम्मी का उर्दू से लगाव इस वजह था क्योंकि यही इकलौती लिपि उन्हें सिखाई गई थी, हालांकि जो भाषा वह बोलती थीं वह थी खालिस अवधी या देहाती. दरअसल, बोली के मामले में लिंगभेद था. ज़्यादातर ख़वातीन अवधी या देहाती बोलतीं मगर औपचारिक मौकों पर उर्दू या हिंदुस्तानी बोल लेतीं. हज़रात उर्दू या हिंदुस्तानी में गुफ़्तगू करते और अनौपचारिक मौकों पर अवधी या देहाती पर आ जाते.
पासपोर्ट, जो नानी अम्मी के लिए हमेशा एक बेहद नापसंद दस्तावेज़ रहा, के बिना ही वह सिधार गईं इस बात में कुछ प्रतीकात्मकता शायद होगी. वह लाहौर में अपनी बेटियों के पास थीं, छह महीनों से बीमार. उनका हिंदुस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चूका था. वह चाहती थीं कि उसे रिन्यू करवाया जाए क्योंकि वह चाहती थीं कि उन्हें मुस्तफ़ाबाद में दफ़नाया जाए. उनकी बेटियों ने उनसे कहा कि यह काम जल्दी ही करवाया जाएगा. मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया. वह एक बेहद ग़मगीन दौर के रूप में मेरी यादों में बसा है. नानी अम्मी के इंतिकाल से हम उबरे ही थे कि अखबारों ने मुरादाबाद (उ.प्र) में 1980 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में दुनिया को बताया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हमेशा की तरह ‘हज़ारों’ बेघर हुए.