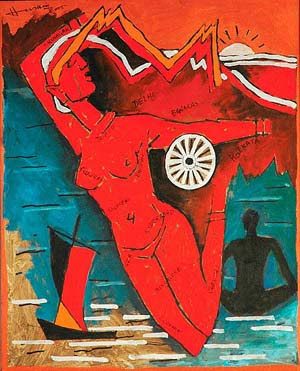पंद्रह नवम्बर २०१७ की शाम दिमाग़ में नक़्श है। लोदी रोड श्मशान में कुँवर नारायण के अंतिम संस्कार के वक़्त अचानक दो लोगों पर नज़र पड़ी−−दीवार के सहारे रखी एक बेंच पर विष्णु खरे अौर केदारनाथ सिंह बैठे थे, नीम अँधेरे में। दोनों बहुत दुर्बल, पस्त अौर लगभग प्राणहीन लग रहे थे, जैसे वहाँ हों ही नहीं, अौर कहते हों कि हमें भी मरा ही जानो। ख़ामोश अभिवादन किया, उन्होंने बड़ी बेज़ारी से सर हिलाया जैसे सरहद पार कर चुके हों। मुझे लगा अब पता नहीं इन्हें दुबारा देख पाऊँगा या नहीं। साल भी न गुज़रा अौर अब वे इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन यह विष्णु खरे से अंतिम ‘संवाद’ न था। इस जून के महीने में यह ख़बर सुनकर कि वह अाम अादमी पार्टी के तहत अाने वाली दिल्ली हिन्दी अकादमी के उप सभापति मनोनीत किये गए हैं, अौर इस तरह वह अपने अज़ीज़ शहर में रहने वापस अा पाएंगे, मैंने उन्हें यह संक्षिप्त ई-मेल संदेश भेजा (२३ जून)−−
“क़िबला, कुछ ख़बर सुनी है। उम्मीद है सच ही निकलेगी। लिहाज़ा बधाई... अौर ख़ुदा ख़ैर करे!”
जल्दी ही उनका मुख़्तसर जवाब अाया−−
“इसमें ‘ख़ुदा ख़ैर करे’ ही operative part [काम की बात] है।”
कम से कम पिछले चालीस साल से हमारे दरमियान संवाद की यही शैली बरक़रार रही। उनसे ऐसी वाक़फ़ियत मेरी ख़ुशक़िस्मती अौर दोस्ती की यह हालत मेरा अभिमान रही। यह ऐसा रिश्ता था जिसमें हम एक दूसरे से बोले कम, नाख़ुश ज़्यादा रहे।
नौ सितम्बर को उन्होँने अपने नये कार्यकाल का पहला काव्यपाठ कराया, जिसमें मैं भी अामंत्रित था। क़रीब दो-ढाई घंटे का साथ रहा। कुछ ख़ामोश लेकिन पुरसुकून नज़र अाते थे। कार्यक्रम के बाद वे जल्द ही अपने अावास के लिए निकल पड़े। दो दिन बाद पता चला ब्रेन हैमरेज के बाद वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। शरीर के एक हिस्से को लकवा मार गया था। हफ़्ते भर की बेहोशी के बाद वह इस दुनिया से चले गए। बहुत सारी बातें अधूरी छूट गईं।
हम जब कविता या कहानी लिखते हैं तो ऐसे कुछ ज़रूरी चेहरे दिमाग़ में रहते हैं जिनके बारे में या तो हमें यक़ीन होता है कि वे हमारे लिखे को पढ़ेंगे या कुछ चिंता होती है कि वे अगर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे। कहीं किसी जगह एक अादमी नज़र रखे हुए है। विष्णु खरे न सिर्फ़ मेरी पीढ़ी के बहुत से कवि-लेखकों के लिए, बल्कि हिन्दी मे सक्रिय बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी, ऐसा ही एक ज़रूरी चेहरा थे। वह कभी हमारे ख़यालों से दूर न रहे। उनका जाना एक , ज़रूरी अादमी का जाना अौर एक दुखद ख़ालीपन का अाना है। मेरी पीढ़ी ने एक अाधुनिक दिमाग़, तेज़ नज़र काव्य-पारखी, अालोचक, दोस्त, स्थायी रक़ीब अौर नई पीढ़ी ने अपना एक ग़ुस्सेवर लेकिन ममतालु सरपरस्त खो दिया है। इस रूप में वह हमारे सबसे क़ीमती समकालीन थे।
चश्म हो तो आईना-ख़ाना है दहर
मुँह नज़र आता है दीवारों के बीच
(मीर)
विष्णु खरे एक अौर घर ख़ाली कर गए हैं, वह घर जो सिर्फ़ उन्हीं के लिए बना था। उसमें कोई अौर नहीं रह सकेगा। कभी उस घर में मीर मेहमान होते थे, कभी मुक्तिबोध, कभी श्रीकांत अौर कभी रघुवीर सहाय। उस घर को बाहर से, उड़ती उड़ती नज़र से ही देखा गया, उस में दाख़िल होना सबके बूते की बात न थी। कविता के उस घर में अावाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, बेचैन रूहें भटकती हैं, वहाँ विषाद है, अार्त्तनाद है, बार बार अपने ही से सामना है, जहाँ कल भी अाज है, अौर विस्मृति है ही नहीं। इस घर में बहुत जंजाल है, क्लेश है, पर कुछ भी अोझल अौर अमूर्त्त नहीं है। कुछ कमरे बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने से वह ख़ुद भी डरते थे, वो अब कभी नहीं खुलेंगे। वह इस मकान के मकीन होकर कम, पहरेदार होकर ज़्यादा रहे। इस घर का नक़्शा उनके जीवनीपरक ब्यौरों से कम उनकी कविताअों से ही झलकता रहेगा।
वह अत्यंत भावुक, संवेदनशील अौर असुरक्षित व्यक्ति थे। अपने इस बुनियादी किरदार को, अपनी वेध्यता को, ढँकने के लिए उन्होंने एक रूखा, अाक्रामक अौर नाटकीय अंदाज़ अपनाया था। उनका यही सार्वजनिक रूप बन गया अौर इसी तर्ज़ के लिए वह जाने गए। उनके अंतरंग मित्र उनके इस स्वाभाव को समझते थे, लिहाज़ा उनकी बहुत सी बातों को नज़रअंदाज़ करते थे। सभी मित्र जहाँ तक बन पड़ता उनकी हिमायत में रहते थे, बेजा अाक्रमण से उनकी हिफ़ाज़त करते थे। वैसे भी विष्णु जी ने मुहब्बत अौर अदावत में कभी ज़्यादा फ़ासला न रखा। यह उन लोगों की कमनज़री है जिन्होंने उनकी ज़्यादतियाँ तो देखीं पर जो उनकी बेरुख़ी अौर ग़ुर्राहट में प्यार अौर हमदर्दी की झलक न देख सके।
विष्णु खरे ने साहित्य जगत में एक तेज़-तर्रार विध्वंसक अालोचक की तरह प्रवेश किया अौर तत्काल ही अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने गए। उनकी ताज़गी, खुले दिमाग़, ज़हानत अौर अध्यवसाय से लोग प्रभावित होते थे। वह अपेक्षाकृत युवा थे अौर उस दौर में युवा होना ख़ुशक़िस्मती की निशानी थी। ऐसा लगता था कि राजनीति, समाज, संस्कृति निर्णायक मोड़ पर है, जो बदलाव अाया चाहता है उसका कार्यभार १९४० के बाद जन्मी पीढ़ी पर है, उसमें अात्मविश्वास है, जोखिम उठाने का जज़्बा है, समस्या वही हल करेगी, उसके पास सारी चाबियाँ मौजूद हैं। १९६४ से १९७५ के बीच का काल भारतीय राजनीति अौर कलाअों में एक प्रकार का मुक्ति प्रसंग था अौर समाज की अंतरात्मा पर कई तरह की दावेदारियाँ सामने अा रही थीं। पहली बार संस्कृति में अवाँगार्द प्रवृत्तियाँ प्रधान प्रवृत्तियों की तरह स्थापित होने लगी थीं। वाम में नव-स्फूर्ति अौर दूरगामी विघटन की प्रक्रियाएँ एक साथ चल रही थीं, गो यह बात उस वक़्त इतनी स्पष्ट न थी। कालांतर में बहुत कुछ एक भोर का सपना ही साबित हुअा। वह दौर जिसे परिवर्तनकारी दौर की तरह देखा जा रहा था, एक लम्बे राष्ट्रीय दुखांत से पहले का अंतराल था। प्रतिभाशाली लोगों की यह पहली खेप नहीं थी जिसकी सामाजिक हस्तक्षेपकारी संभावनाएँ मूर्त्तिमान नहीं हो सकीं अौर उनकी अपनी क्षमता अौर ताक़त संस्थानों अौर प्रतिष्ठानों के भीतर ही जज़्ब होकर या अपना स्थान वहाँ बनाए रखने में ही ख़र्च होकर रह गई। विष्णु खरे इसका अपवाद न थे।
विष्णु खरे हरदम संस्कृति अौर साहित्य की दुनिया में रमे रहकर खप जाना चाहते थे। उनके दौर के हालात साज़गार नहीं थे, अौर न सिर्फ़ उनका स्वभाव बल्कि उनकी वैचारिक प्रेरणाएँ भी रास्ते में अाती थीं। लेकिन सांस्कृतिक परिदृश्य में केन्द्रीय अौर निर्णायक भूमिका निभाने की उनकी तीव्र इच्छा उन्हें एक ग़लत जगह ले गई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हस्तिनापुर कॉलेज (अब मोतीलाल नेहरू कॉलेज) में अंग्रेज़ी अध्यापक की स्थायी नौकरी छोड़कर साहित्य अकादमी के उप-सचिव पद के लिए अावेदन देने की ठान ली। भारतभूषण अग्रवाल ने भी उन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया। एक रोज़ उन्होंने अपनी जीवनसाथी कुमुद को स्कूटर पर बिठाया अौर दोनों ख़ुशी ख़ुशी भारतभूषण जी के पास गए अौर उन्हीं को अावेदन देकर अा गए। वह एक संभावनामय, सार्थक अौर उज्ज्वल भविष्य की अोर नहीं, बल्कि अँधेरे में छलाँग लगा रहे थे। १९७६ में वह साहित्य अकादमी के उप-सचिव तैनात हुए। उस समय उनकी उम्र ३६ साल थी। मैं बाईस तेईस साल का था अौर उद्दंडता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता था। उसी साल या शायद उससे अगले साल एक रोज़ मैंने उनसे पूछा, “अापको संस्कृति प्रशासक बनने का इतना शौक़ कैसे पैदा हुअा? अध्यापकी में जो अाज़ादी अौर गरिमा है उसे लात मारकर कहाँ ये साहित्य अकादेमी में अा फँसे? अापको बहुत समझौते करने पड़ेंगे।” विष्णु खरे ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा अौर एक क्रुद्ध साँड की तरह डकराए—“हुँह!” ज़ाहिर है उन्हें कोई मलाल न था। उन्होंने कुछ इस इस तरह की बात कही कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या करने बैठा हूँ? मैंने कहा, खरे जी, यह जगह अौसतपन (मीडियॉक्रिटी) का गढ़ है। अाप नष्ट हो जाएँगे। बोले, तुम कह रहे हो मैं यहाँ अौसत काम करूँगा। मैंने कहा, देख लीजिएगा। उन्होंने कुछ स्नेह अौर कुछ नाराज़ी से कहा, “तुम्हें तुम्हारी ये काली ज़बान बहुत कष्ट देगी। तुम जे एन यू में हो। वहाँ वो नामवर भी है... उससे बचके रहना।”
मुझे अाज तक इस बातचीत पर अफ़सोस अौर ग्लानि है। अपनी धृष्टता पर, अौर इस बात पर कि मेरी ‘काली ज़बान’ से अनायास जो बात निकली थी वह एक तरह की भविष्यवाणी साबित हुई। साहित्य अकादेमी के कार्यक्रम प्रभारी वाले अपने कार्यकाल में उनके सम्पर्क अखिल भारतीय साहित्यिक अभिजन या श्रेष्ठिवर्ग अौर देशी विदेशी साहित्य संस्थानों अौर मंडलियों से अौर दूतावासों से बढ़े, अनुवाद का काम तलाशते बेरोज़गारों को छिटपुट काम दिला सके, छोटे प्रकाशकों अौर छापेख़ानों के मालिक उनके चक्कर लगाते थे, इस रुसूख़ की वजह से नए कवियों के कविता संग्रह छपाने में मददगार हुए, कविता-कहानी लिखने वाले प्रशासनिक सेवाअों में सक्रिय नौकरशाहों से बराबरी से बात करने की सुविधा प्राप्त हुई। सबसे बड़ी बात यह हुई कि साहित्य अकादेमी की अाला अफ़सरी की वजह से हिन्दी के अाचार्यगण अौर पिछड़ी समझ के लेखक कवि अब उनकी कविता को कुछ मान्यता देने लगे। लेकिन कुल मिलाकर उनके जीवन के इतने सारे वर्ष वहाँ बरबाद ही हुए। एक बुद्धिजीवी, चिंतक अौर लेखक के रूप में उनका विकास अवरुद्ध हुअा। अौर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कों का अौर हिन्दी की व्यावसायिक दुनिया से संबंधों का यह जाल मायाजाल ही साबित हुअा। ये सम्पर्क अौर लगातार विस्तारमान दिखती दुनिया अंततः कामकाजी दुनिया थी, वे संबंध भी कामकाजी अौर रस्मी ही थे। वह उनकी कॉन्स्टीटुएन्सी थी ही नहीं। जब तक महफ़िल गर्म थी, उन्हें अच्छा लगता रहा। अकादेमी से जब हटे तो यह दुनिया सिकुड़ गई। संस्कृति के महाबली बनने का उनका सपना कब का ख़त्म हो चुका था। मातहती उन्हें अाती न थी, बिना मातहती के अाज की दुनिया में महाबली कोई बन नहीं सकता।
उनकी दूसरी भूल थी यह समझना कि वह हिन्दी पत्रकारिता में कुछ परिवर्तन ला पाएँगे। टाइम्स ग्रुप में वह ऐसे समय नौकरी करने लगे जब अख़बार की दुनिया में समीर जैन-विनीत जैन का अभ्युदय हो चुका था, अौर पत्रकारिता एक बुद्धिविरोधी, मुजरिमाना दौर में प्रवेश कर चुकी थी। एक पेशे के रूप में भी पत्रकारिता का महत्त्व गिर रहा था, संपादकी का दरजा घट रहा था अौर काम की शर्तें पत्रकारों के विरुद्ध बदली जा रही थीं। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया जा रहा था। ऐसे समय में मैनेजमेंट के साथ होना इस प्रक्रिया की पैरोकारी करना अौर इसमें मालिकान का हाथ बटाना ही था, जो काम (मुझे खेद है कि) सुरेन्द्रप्रताप सिंह जैसे संपादकों ने जमकर किया। इस दौर में बहुत से उपयोगी लफंगे पत्रकारिता में घुसे, अौर अख़बारों में उनका महत्त्व बढ़ता गया। ऐसे ही दौर में दिल्ली, लखनऊ, जयपुर में सम्पादकी करने के बाद विष्णु खरे पत्रकारिता से बाहर अाए। ज़िंदगी के इतने साल फिर से बरबाद करके। वह ख़ुद कहते थै ‘मॉय ट्रिस्ट विद जर्नलिज़्म वाज़ अ फ़िअास्को।’ अौर सही ही कहते थे।
इस दौर के बाद का उनका जीवन एक फ़्री-लांसर का जीवन था, जो कि हिन्दी में कोई जीवन ही नहीं हैं। पेशेवरी के ऐतबार से अनुवादक का जीवन भी, जैसा कि सब जानते हैं, कोई जीवन नहीं है, अौर फ़िल्म समीक्षक या फ़िल्म अालोचक का जीवन भी कोई जीवन नहीं है। इस दौर में जो काम उन्होंने किये अच्छे ही किए, पर मुझे संदेह है कि अपनी प्राथमिकता से किए। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसी अवांछनीय जिरहें भी कीं जो अगर वह न करते तो हिन्दी के एक रौशनख़याल, सेकुलर नज़रिए पर जीवन भर अडिग रहने वाले अादमी के रूप में उनकी छवि को नुक़सान न पहुँचता। मैं तो यही समझता हूँ कि पिछले पंद्रह बीस साल में उन्होंने साहित्यिक परिदृश्य, ख़ासकर काव्य परिदृश्य, में विराट हस्तक्षेप अौर कॉन्स्टीटुएन्सी बिल्डिंग की जो कोशिशें कीं, उनके पीछे कोई सुचिंतित ख़ाका, गहरी कल्पनाशीलता या गहन सौंदर्यशास्त्रीय चिंतन न था। उनके व्यक्तित्त्व में एक मुक्तिबोधीय पहलू ज़रूर था, जिसकी मांग वह पूरी न कर सके। इसका उन्हें अहसास था, ऐसा मुझे लगता है।
मुझे उनको देखकर हमेशा श्रीकांत वर्मा की याद अाई। वही बेचैनी, वैसी ही महत्त्वाकांक्षा, वैसा ही फ़्रस्ट्रेशन। उन्हें ताक़त अाज़माना अाता था लेकिन ताक़त का माक़ूल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे—उसके प्रदर्शन में ही उनका वक़्त निकल जाता था। न वह अच्छे बॉस थे, न अच्छे मातहत। पूरा जीवन संशय अौर दुविधा से भरा था पर वह कभी यह क़ुबूल नहीं करते थे। ऐसा वक़्त भी था — अौर बीच बीच में अभी तक अाता रहा — जब विष्णु खरे को एक कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी या सिक्काबंद वामपंथी की तरह देखा गया। अक्सर उन्हें ख़ुद भी शौक़ होता था कि उनको प्रतिबद्ध वामपंथी कहा जाए। पर इससे जो ज़िम्मेदारी अान पड़ती है उसे उठाना उनके बस में कभी न रहा। इन दोनों—श्रीकांत अौर विष्णु—पर मुक्तिबोध का साया पड़ा था। वह साया जीवन भर उनके साथ लगा रहा—वे जानते थे वे किसके प्रति जवाबदेह हैं। इनके अंतःकरण में मुक्तिबोध मौजूद थे। वे यह भी जानते है कि उनके लिए यह वरदान नहीं अभिशाप है। वे इसी अंतःकरण में मुक्तिबोधियन शाप झेलने को अभिशप्त हैं। यह कोई निन्दा नहीं, इनके व्यक्तित्त्व अौर कृतित्त्व के मर्म को समझने का प्रयास है। कम से कम विष्णु खरे को ख़ुद इस धारणा से ऐतराज़ न था। एक बार इसी ‘मुक्तिबोधियन कर्स’ पर कुछ बात हुई। वह अचानक विचलित हुए, ठंडी साँस भरकर बोले—‘हाँ भई…’ अौर चुप हो गए।
यह सब मैं इसलिए कहता हूँ कि १९७० के दशक में विष्णु खरे हिन्दी साहित्य अौर संस्कृति जगत के भावी अौर समर्थ नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। ही वाज़ द नेक्स्ट बिग होप। वह मेरे भी हीरो थे। वह एक अाला दर्जे का चिंतक, साहित्येतिहास लेखक, सिद्धांतकार हो सकते थे, किसी हद तक थे भी, लेकिन बेशतर काम वह किए बिना चल बसे। बेशक उनकी ये असफलताएँ या विवशताएँ हममें से बहुतों की सफलताअों से तो बेहतर ही हैं। उनकी समस्या यह थी कि वह सत्ता, रुतबे, सरपरस्ती या संस्थान से जुड़े बिना कुछ करना पसंद नहीं करते थे। सिर्फ़ अपने दम पर कुछ पहल लेने को वह अपने अात्मसम्मान के ख़िलाफ़ समझते थै। एक तरह के विद्रोही होने के बावुजूद उन्हें सत्ता या इक़्तिदार का मोह भी था जो कि मेरी पीढ़ी के लोगों में भी कम नहीं हैं, अलबत्ता उनकी विष्णु खरे जैसी पहुँच नहीं है।
 यह मुहब्बतनामा कुछ जल्दी में लिखा गया है। अौर अच्छा ही है कि जल्दी ने कुछ लिखवा लिया अौर दुबारा ग़ौर करने का मौक़ा संपादक ने न दिया। बहरहाल मौसूफ़ ज़िंदा होते तो इसमें मीन मेख़ ज़रूर निकालते, पर कुल मिलाकर इसे मुहब्बतनामा ही जानते।
यह मुहब्बतनामा कुछ जल्दी में लिखा गया है। अौर अच्छा ही है कि जल्दी ने कुछ लिखवा लिया अौर दुबारा ग़ौर करने का मौक़ा संपादक ने न दिया। बहरहाल मौसूफ़ ज़िंदा होते तो इसमें मीन मेख़ ज़रूर निकालते, पर कुल मिलाकर इसे मुहब्बतनामा ही जानते।(‘समयान्तर’ में `एक और खाली घर` शीर्षक से प्रकाशित। वहीं से साभार)